प्रेमचंद होते तो खिन्न, लेकिन संघर्षरत होते… – अशोक कुमार पांडेय
 प्रेमचंद जिस समय लिख रहे थे वह औपनिवेशिक शासन का समय था. वह शासन जो अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए ही स्थापित हुआ था और जिसे इस देश को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाना था. कृषि व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया गया और अठारहवीं सदी राजकीय संरक्षण में ज़मीन की लूट खसोट की सबसे भयानक घटनाओं की प्रत्यक्षदर्शी बनी.
प्रेमचंद जिस समय लिख रहे थे वह औपनिवेशिक शासन का समय था. वह शासन जो अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए ही स्थापित हुआ था और जिसे इस देश को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाना था. कृषि व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया गया और अठारहवीं सदी राजकीय संरक्षण में ज़मीन की लूट खसोट की सबसे भयानक घटनाओं की प्रत्यक्षदर्शी बनी.
लेकिन इसी के बरअक्स आज़ादी की लड़ाई के साथ पलता वह स्वप्न भी था कि अपना राज जब आयेगा तो यह दुःख दूर होगा, आखिरी आदमी तक पहुंचेगी मुस्कान और एक बराबरी वाले सर्वकल्याणकारी समाज की स्थापना होगी. उनका किसान इसी अत्याचार की मार झेलता और इस स्वप्न को जीता किसान था. एक तरफ अत्याचारी शासन तो दूसरी तरफ अपने ही समाज का वह बर्बर ढाँचा जो उसे जाति की अमानवीय श्रेणियों में बांटकर निष्ठुर कर्मकांडों और क्रूर परम्पराओं की जंज़ीरों में ऐसा कसे हुए था कि एक एक साँस लेनी मुश्किल थी. इन हालात कि एक पैदाइश था हल्कू जो पूस की रात किसानी से जान छूटने से संतोष पाता है और मज़दूरी करने का तय करता है तो एक पैदाइश वे घीसू माधव भी थे जिन्होंने हाड़ तोड़ मेहनत के फल के बारे में ठीक ठीक जान लिया था और उन परम्पराओं के मासूम फ़ायदे उठाना सीख लिया था.
तो प्रेमचंद ने लिखते हुए एक तरफ इस किसान के दुःख दर्द और सामजिक-आर्थिक विडम्बनाओं को एकदम सीधे सीधे दर्ज किया तो दूसरी तरफ उस समय की राजनीतिक सामजिक जीवन की साम्प्रदायिकता, जाति प्रथा, आर्थिक विषमता आदि को भी कहानियों में ही नहीं बल्कि अपने लेखों में भी दर्ज किया और साथ ही अपनी प्रतिबद्धता भी साफ़ की. यह उनकी सफलता है कि वे आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन हमारे समाज और राजनीति की विफलता है.
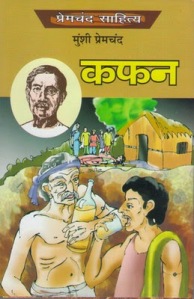 आज अगर वह होते तो ज़ाहिर तौर पर उस समय से अधिक उद्विग्न होते कि मुसीबतें तो नए नए रूपों में सामने उपस्थित हैं लेकिन स्वप्न सारे खंडित. दूर तक निगाह में कोई नवनिर्माण का दृश्य नहीं दीखता. आजादी के बाद जो उम्मीद थी "अपने" शासकों से उसका शतांश भी पूरा नहीं हुआ. नब्बे का दशक शासकीय नीतियों के लगातार पूंजीपतियों के पक्ष में झुकते जाने और इसके साथ साथ साम्प्रदायिकता के उभार का दशक था और यह प्रक्रिया सत्ताओं के परिवर्तनों के बावजूद अब तक ज़ारी है. वह होते तो खिन्न होते पर संघर्षरत होते. आज भी बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहने से नहीं रुकते.
आज अगर वह होते तो ज़ाहिर तौर पर उस समय से अधिक उद्विग्न होते कि मुसीबतें तो नए नए रूपों में सामने उपस्थित हैं लेकिन स्वप्न सारे खंडित. दूर तक निगाह में कोई नवनिर्माण का दृश्य नहीं दीखता. आजादी के बाद जो उम्मीद थी "अपने" शासकों से उसका शतांश भी पूरा नहीं हुआ. नब्बे का दशक शासकीय नीतियों के लगातार पूंजीपतियों के पक्ष में झुकते जाने और इसके साथ साथ साम्प्रदायिकता के उभार का दशक था और यह प्रक्रिया सत्ताओं के परिवर्तनों के बावजूद अब तक ज़ारी है. वह होते तो खिन्न होते पर संघर्षरत होते. आज भी बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहने से नहीं रुकते.
वह नहीं हैं..और हम हैं. खुद को उनकी परम्परा का कहने वाले. ज़रा झाँक ले अपने मन में और पूछें कहीं सच में बिगाड़ के डर बेईमानी तो नहीं करने लगे हैं हम?
 अशोक कुमार पांडेय
अशोक कुमार पांडेयइस टिप्पणी के लेखक, दखल प्रकाशन के ज़रिए जनवादी और चेतनामूलक साहित्य का प्रचार-प्रसार करने में लगे हैं। अशोक कुमार पांडेय के दो कविता संकलन प्रलय में लय कितना समेत, मार्क्स पर एक सामयिक दृष्टि की किताब और निबंधों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। विभिन्न पत्रिकाओं का सम्पादन और अतिथि सम्पादन किया है।
No comments:
Post a Comment